अदालत की अवमानना; एक अंतर्दृष्टि चर्चा
अवमानना की परिभाषा
1- किसी न्यायाधीश या जज के खिलाफ निन्दात्मक या विद्वेषपूर्ण वक्तव्य अथवा प्रकाशन द्वारा उसे पद की गरिमा को अयोग्य कहना या लांछन लगाना या उसके पदीय गौरव के खिलाफ आघात करना, या किसी न्यायालय के फैसले खिलाफ निन्दात्मक या विद्वेषपूर्ण वक्तव्य देना अथवा प्रकाशित करना
2- न्यायालय में विचाराधीन मामले के बारे में जनता के मन में भ्रम या पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रकाशन
3- न्यायालय में किसी विचाराधीन मामले में जज, पक्षकार, साक्षी पर आक्षेप अथवा उनपर प्रभाव डालने का प्रयत्न करना
4- किसी प्रकाशन के कारण न्यायलय के प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा खड़ी करना
अवमानना के प्रकार
अदालती अवमानना दो प्रकार हो सकते हैं
सिविल
फौजदारी
पहली अवमानना का संबंध किसी निर्णय या निर्देश की अवमानना से है । दूसरी अवमानना का अर्थ लिखे या बोले गए शब्द या संकेत कार्य से है , जो किसी न्यायालय के अधिकार और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है या जिसमें ठेस पहुंचाने की प्रवृति होती है ।
यहां एक बात याद रखने लायक है कि किसी अदालती कार्यवाही की सही और संतुलित रिपोर्ट के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सैद्धांतिक आधार पर संतुलित एवं वेवकपरक टिप्पणी के लिए भी किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।
अवमानना के लिए सजा
अदालत अवमानना के लिए छह महीने का साधारण कारावास तथा दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है । या किसी व्यक्ति को दोनों ही सजा सुनाई जा सकती है । अदालत के समक्ष संतोषप्रद क्षमायाचना की स्थिति में अभियुक्त से सजा से मुक्त किया जा सकता है ।
सजा देने का अधिकार
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए न्यायालय को स्वयं उस मामले की सुनवाई करने का तथा सजा देने का आधिकार है । फौजदारी अवमानना के लिए सर्वोच्च न्यायलय या उच्च न्यायालय स्वयं कार्यवाही करने का अधिकारी है , या एेसी कार्यवाही के लिए महाधिवक्ता या महाधिवक्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति के आवेदन की अपेक्षा होती है । अवमानना की तिथि से एक वर्ष के भीतर अवमानना के विषय के कार्यवाही शुरू करने की अवधि है । ( आधार- विधि पत्रकारिता: चिंता और चुनौती, लेखक-पवन चौधरी मनमौजी)




















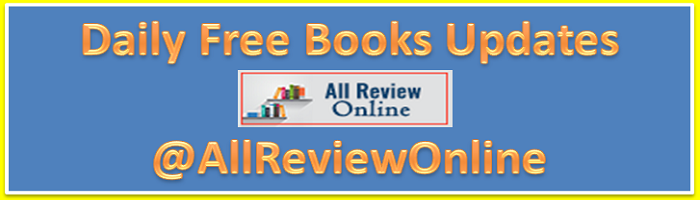
i must congrats for ur article ...u did grt work ...spl the topic ...its tooo gud...keep helping #happylearning
ReplyDeleteThank you so much. yes, I will do.
Delete